

30,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today
Here’s your new year gift, one app for all your, study abroad needs, start your journey, track your progress, grow with the community and so much more.

Verification Code
An OTP has been sent to your registered mobile no. Please verify

Thanks for your comment !
Our team will review it before it's shown to our readers.

रिसर्च डिज़ाइन क्या है?
- Updated on
- नवम्बर 14, 2022
विज्ञान और टेक्नोलॉजी, कला और संस्कृति, मीडिया अध्ययन, भूगोल, गणित और अन्य विषय हों, रिसर्च हमेशा अज्ञात को खोजने का मार्ग रहा है। वर्तमान निराशाजनक परिस्थितियों में जब कोरोनावायरस ने दुनिया को तहस-नहस कर दिया है, इसके इलाज के लिए टीके खोजने के लिए भारी मात्रा में रिसर्च किया जा रहा है। इस ब्लॉग में, हम समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन और उनके संबंधित फैक्टर क्या है।
This Blog Includes:
एक रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च डिज़ाइन के लाभ, रिसर्च डिजाइन के तत्व, रिसर्च डिजाइन की विशेषताएं, ग्रुपिंग द्वारा रिसर्च डिज़ाइन प्रकार, जनसंख्या वर्ग स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लोंगिट्यूडनल स्टडी, क्रॉस-सेक्युएंशियल स्टडी, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, फिक्स्ड बनाम फ्लेक्सिबल रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिज़ाइन ppt.
शोध’ शब्द से, हम समझ सकते हैं कि यह डेटा का एक कलेक्शन है जिसमें रिसर्च मेथड्स को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। दूसरे शब्दों में, यह एक हाइपोथिसिस स्थापित करके खोजी गई जानकारी या डेटा का संकलन (कंपाइलेशन) है और इसके परिणामस्वरूप एक संगठित तरीके से वास्तविक निष्कर्ष सामने आता है। रिसर्च अकादमिक के साथ-साथ वैज्ञानिक आधार पर भी किया जा सकता है। आइए पहले समझते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन का वास्तव में क्या अर्थ है।
रिसर्च डिजाइन एक रिसर्चर को अज्ञात में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है लेकिन उनके पक्ष में एक सिस्टेमेटिक अप्रोच के साथ। जिस तरह से एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट एक स्ट्रक्चर के लिए एक डिजाइन तैयार करता है, उसी तरह रिसर्चर विभिन्न तरीकों से डिजाइन को चुनता है, ताकि यह जांचा जा सके कि किस प्रकार का रिसर्च किया जाना है।
रिसर्च डिज़ाइन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
- एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करने से रिसर्चर को अध्ययन के प्रत्येक चरण में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- यह अध्ययन के प्रमुख और छोटे कार्यों की पहचान करने में मदद करता है।
- यह शोध अध्ययन को प्रभावी और रोचक बनाता है।
- इससे एक रिसर्चर आसानी से शोध कार्य के उद्देश्यों को तैयार कर सकता है।
- एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन का मुख्य लाभ यह है कि यह शोध को संतुष्टि,आत्मविश्वास, एक्यूरेसी, रिलियाबिलिटी, कंटीन्यूटी और वैलिडिटी प्रदान करता है।
- इसके द्वारा लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सभी कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
- इससे रिसर्च में कम समय लगता है।
यहाँ एक रिसर्च डिज़ाइन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं:
- एकत्रित विवरण का एनालिसिस करने के लिए लागू की गई विधि
- रिसर्च मेथड का प्रकार
- सटीक उद्देश्य कथन
- शोध के लिए संभावित आपत्तियां
- रिसर्च के संग्रह और एनालिसिस के लिए लागू की जाने वाली तकनीकें
- एनालिसिस का मापन
- शोध अध्ययन के लिए सेटिंग्स

रिसर्च डिजाइन के प्रकार
अब जब हम व्यापक रूप से क्लासीफाइड प्रकार के रिसर्च को जानते हैं, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रकार के research design in Hindi में विभाजित किया जा सकता है-
- डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन
- कॉरिलेशनल रिसर्च डिजाइन
- एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन
- डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन
- एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन
अध्ययन डिजाइन प्रकारों का एक अन्य क्लासिफिकेशन इस पर आधारित है कि प्रतिभागियों को कैसे क्लासीफाइड किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में, समूहीकरण रिसर्च के आधार और व्यक्तियों के नमूने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन के आधार पर एक विशिष्ट अध्ययन में आम तौर पर कम से कम एक प्रयोगात्मक और एक नियंत्रण समूह होता है। चिकित्सा रिसर्च में, उदाहरण के लिए, एक समूह को चिकित्सा दी जा सकती है जबकि दूसरे को कोई नहीं मिलता है। तुम मेरा फॉलो समझो। हम प्रतिभागी समूहन के आधार पर चार प्रकार के अध्ययन डिजाइनों में अंतर कर सकते हैं:
एक को होर्ट अध्ययन एक प्रकार का अनुदैर्ध्य रिसर्च है जो पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर एक समूह के क्रॉस-सेक्शन (एक सामान्य लक्षण वाले लोगों का एक समूह) लेता है। यह पैनल रिसर्च का एक रूप है जिसमें समूह के सभी लोगों में कुछ न कुछ समान होता है।
सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा रिसर्च और जीव विज्ञान में, एक क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन प्रचलित है। यह अध्ययन दृष्टिकोण किसी विशिष्ट समय पर जनसंख्या या जनसंख्या के प्रतिनिधि नमूने के डेटा की जांच करता है।
एक अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें एक ही चर को कम या लंबी अवधि में बार-बार देखा जाता है। यह आमतौर पर अवलोकन संबंधी शोध है, हालांकि यह दीर्घकालिक रेंडम प्रयोग का रूप भी ले सकता है।
क्रॉस-अनुक्रमिक रिसर्च डिजाइन अनुदैर्ध्य और क्रॉस-अनुभागीय रिसर्च विधियों को जोड़ती है, दोनों में निहित कुछ दोषों की कंपनसेशन के लक्ष्य के साथ।
क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव research design in Hindi के बीच अंतर निम्नलिखित हैं-
स्थिर और फ्लेक्सिबल research design in Hindi के बीच एक अंतर भी खींचा जा सकता है। क्वांटिटेटिव (निश्चित डिजाइन) और क्वालिटेटिव (लचीला डिजाइन) डेटा एकत्र करना अक्सर इन दो अध्ययन डिजाइन श्रेणियों से जुड़ा होता है। आपके द्वारा डेटा एकत्र करना शुरू करने से पहले ही रिसर्च डिज़ाइन एक निर्धारित अध्ययन डिजाइन के साथ पूर्व-निर्धारित और समझा जाता है। दूसरी ओर, लचीले डिज़ाइन, डेटा संग्रह में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं – उदाहरण के लिए, आप निश्चित उत्तर विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उत्तरदाताओं को अपने स्वयं के उत्तर देने होंगे।
Research design in Hindi के लिए PPT नीचे दी गई है-
चूंकि हम रिसर्च डिज़ाइन के प्रकारों से निपट रहे हैं, इसलिए यह समझना अनिवार्य है कि रिसर्च करने का अभ्यास कितना फायदेमंद है और इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं: 1. रिसर्च विषय की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करता है। 2. आप इसके विविध पहलुओं के साथ-साथ इसके विभिन्न स्रोतों जैसे प्राथमिक और माध्यमिक के बारे में जानेंगे। 3. यह महत्वपूर्ण एनालिसिस और अनसुलझी समस्याओं के मापन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। 4. आप यह भी जान पाएंगे कि संरक्षित मान्यताओं को तौलकर एक परिकल्पना कैसे बनाई जाती है।
रिसर्च ‘ शब्द से, हम समझ सकते हैं कि यह डेटा का एक संग्रह है जिसमें शोध पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। दूसरे शब्दों में, यह एक परिकल्पना स्थापित करके खोजी गई जानकारी या डेटा का संकलन है और इसके परिणामस्वरूप एक संगठित तरीके से वास्तविक निष्कर्ष सामने आता है।
यहाँ एक रिसर्च डिज़ाइन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है: 1. एकत्रित विवरण का एनालिसिस करने के लिए लागू की गई विधि 2. रिसर्च पद्धति का प्रकार 3. सटीक उद्देश्य कथन 4. रिसर्च के लिए संभावित आपत्तियां 5. रिसर्च के संग्रह और एनालिसिस के लिए लागू की जाने वाली तकनीकें 6. समय 7. एनालिसिस का मापन 8. रिसर्च स्टडीज के लिए सेटिंग्स
एक सुनियोजित शोध डिजाइन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके तरीके आपके शोध के उद्देश्यों से मेल खाते हैं, कि आप उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा एकत्र करते हैं, और यह कि आप विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही प्रकार के विश्लेषण का उपयोग करते हैं । यह आपको वैध, भरोसेमंद निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है।
रिसर्च के 5 घटक परिचय, साहित्य समीक्षा, विधि, परिणाम, चर्चा, निष्कर्ष है ।
उम्मीद है कि रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। यदि आप रिसर्च डिजाइन करना चाहते हैं तो Leverage Edu एक्सपर्ट्स के साथ 30 मिनट का फ्री सेशन 1800 572 000 बुक करें और बेहतर गाइडेंस पाएं।
देवांग मैत्रे
स्टडी अब्रॉड फील्ड के हिंदी एडिटर देवांग मैत्रे को कंटेंट और एडिटिंग में आधिकारिक तौर पर 6 वर्षों से ऊपर का अनुभव है। वह पूर्व में पोलिटिकल एडिटर-रणनीतिकार, एसोसिएट प्रोड्यूसर और कंटेंट राइटर रह चुके हैं। पत्रकारिता से अलग इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी काम करने का अनुभव है। देवांग को काम से अलग आप नियो-नोयर फिल्म्स, सीरीज व ट्विटर पर गंभीर चिंतन करते हुए ढूंढ सकते हैं।
प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें
अगली बार जब मैं टिप्पणी करूँ, तो इस ब्राउज़र में मेरा नाम, ईमेल और वेबसाइट सहेजें।
Contact no. *

Leaving already?
8 Universities with higher ROI than IITs and IIMs
Grab this one-time opportunity to download this ebook
Connect With Us
30,000+ students realised their study abroad dream with us. take the first step today..

Resend OTP in

Need help with?
Study abroad.
UK, Canada, US & More
IELTS, GRE, GMAT & More
Scholarship, Loans & Forex
Country Preference
New Zealand
Which English test are you planning to take?
Which academic test are you planning to take.
Not Sure yet
When are you planning to take the exam?
Already booked my exam slot
Within 2 Months
Want to learn about the test
Which Degree do you wish to pursue?
When do you want to start studying abroad.
September 2024
January 2025
What is your budget to study abroad?
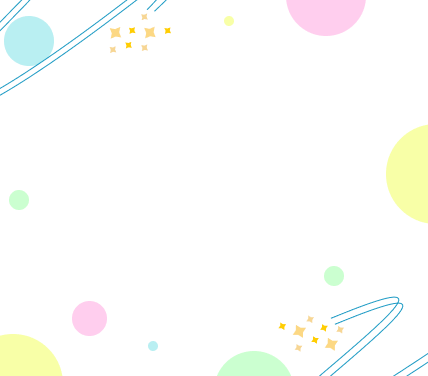
How would you describe this article ?
Please rate this article
We would like to hear more.

- मुखपृष्ठ
- कर्मकाण्ड
- वास्तुशास्त्र
- ज्योतिष
- अनुसन्थान
- काव्यशास्त्र
- भागवत रहस्य
- भागवत पाठ
- प्रश्नोत्तरी
- वैदिक कथाएँ
- शोधप्रारूप(synopsis) कैसे बनाएँ ? how to create a research design ?

जब हम अपने रिसर्च कार्य का प्रारम्भ करते है तो सबसे पहले शोध विषय(research topic) का चयन करते है । शोध विषय का निश्चय करने के तुरन्त बाद यह प्रश्न आता है कि इस शोधकार्य का प्रयोजन क्या है ? तथा कैसे इस शोध कार्य को पूर्ण करना है? यही तथ्य एक प्रक्रिया के द्वारा लिखित रूप में अपने गाइड और कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है जिसे हम शोधप्रारूप या सिनॉप्सिस(synopsis) कहते हैं।
शोधप्रारूप या सिनॉप्सिस(synopsis) सही ढंग से न प्रस्तुत करने के कारण वर्षों तक यहाँ-वहाँ भटकना पड़ता है तथा शोधकार्य पिछड़ता चला जाता है।दोस्तों यदि आपने शोधप्रारूप का निर्माण सही ढंग से कर लिया याकि एक बेहतर तरीके से चरणबद्ध शोधप्रारूप सिनॉप्सिस(synopsis) निर्मित कर ली तो यह कमेटी से शीघ्र ही पास हो जाता है । इसलिए कभी भी शोधप्रारूप का निर्माण चरणबद्ध तरीके से करें । शोधप्रारूप निर्माण के कुछ चरण निर्धारित किये गये हैं जिससे शोधप्रारूप बनकर तैयार होता है ।
शोधप्रारूप के 10 चरण(ten stages of research design)
1. परिचय पृष्ठ(introduction page), 2. प्रस्तावना(preface).
3. औचित्य(justification)
4. प्रयोजन(purpuse of research)
5. प्राक्कल्पना(hypothesis)
6. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि(historical background).
7. शोध सर्वेक्षण(research survey)
8. शोध प्रकृति(nature of research)
9. अध्याय विभाजन(chapter division)
10. सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची(reference bibliography)
शोधप्रारूप या सिनॉप्सिस(synopsis) के यही दस चरण हैं जिससे शोधप्रारूप का निर्माण होता है । अब हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे ।
यह सिनॉप्सिस(synopsis) का पहला पेज(front page) होता है जिसमें निम्नलिखित सूचनाएँ देते हैं-
- युनिवर्सिटी का लोगो(logo) तथा युनिवर्सिटी का नाम(name of university)
- शोध-विषय(research topic)
- सत्र(year)
- शोधनिर्देशक/निर्देशिका (name of superviser or guide)
- अपना नाम(your name)
प्रस्तावना वह भाग होता है जिसमें अपने शोध शीर्षक के विषय में सामान्य जानकारी देनी पड़ती है । एक तरह से यह आपके शीर्षक का सामान्य परिचय होता है । प्रस्तावना बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए । एक-एक शब्द को अच्छी तरह से जाँच-परखकर रखना चाहिए । प्रस्तावना में 300 से 500 शब्द होने चाहिए । आवश्यकतानुसार इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है । परन्तु ध्यान रहे प्रस्तावना में व्यर्थ बातें नहीं भरनी चाहिए । जो आवश्यक बातें हो वही इस भाग में लिखें ।
3. औचित्य(justification)
आप जिस शीर्षक पर कार्य करने जा रहे हैं उस शीर्षक का औचित्य क्या है ? इसके बारे में यहाँ लिखना होता है। औचित्य का आशय यह है कि जिस विषय का आपने चयन किया है उस पर शोधकार्य करने की आवश्यकता क्या है । आपके इस शोधकार्य के करने से कौन-कौन सी नई बातें निकलकर आएंगी जिसके बारे में जानना जरूरी है। कभी-कभी हमें लगता है कि औचित्य और प्रयोजन एक ही बात है पर ऐसा नहीं है, इसमें अन्तर है । औचित्य भाग में केवल आपके शोध कार्य की आवश्यकता से सम्बन्धित बातों का जिक्र होता है जबकि प्रयोजन भाग में शोधकार्य के फल या परिणाम की जानकारी दी जाती है। अतः इन दोनों का अन्तर समझकर पृथक-पृथक जानकारी लिखनी चाहिए । इस भाग में यह भी बताना होता है कि इस विषय पर कितना कार्य हुआ है और क्या बाकी है । जो भाग शेष है उसकी भी पूर्ण जानकारी इसमें लिखनी चाहिए । क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस विषय पर आप कार्य करने जा रहे हैं उस पर कार्य हुआ होता है परन्तु आपको लगता है कि नहीं यह कार्य अभी पूर्ण नहीं है , इसमें इतना भाग बचा है जिस पर शोधकार्य होना चाहिए। इसी बात की जानकारी इस भाग में देनी पड़ती है ।
4. प्रयोजन(Purpose of research)
आपके शोधकार्य का कोई न कोई प्रयोजन होना चाहिए । जैसा कि कहा गया है -
प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते॥
अतः आपके शोधशीर्षक में एक अच्छा परिणाम, फल या प्रयोजन छुपा होना चाहिए । बिना प्रयोजन के शोध शीर्षक का चयन नहीं करना चाहिए । इस भाग में यह लिखना होता है कि आपने जो शोध शीर्षक चुना है उसका प्रयोजन क्या है ? इस शोधकार्य का परिणाम क्या होगा ? इसका जिक्र इस भाग में करना चाहिए । ध्यान रहे आपके शोध शीर्षक के विस्तार के आधार पर ही प्रयोजन का निश्चय करना चाहिए । ऐसा न हो कि जो प्रयोजन आप दिखा रहे हों वहाँ तक आपके शोध शीर्षक की पहुँच ही न हो । जैसे आपने किसी एक साहित्यिक पुस्तक पर शोधकार्य आरम्भ किया तथा प्रयोजन में लिखा कि इस शोधकार्य से सम्पूर्ण साहित्य जगत् का कल्याण होगा । यह गलत है । साहित्य जगत् बहु-विस्तृत शब्द है । एक पुस्तक पर किया गया कार्य समग्र साहित्य का कल्याण नहीं कर सकता अतः आपके द्वारा दिखाया गया यह प्रयोजन निरर्थक है । इस विषय का सही प्रयोजन यह है कि प्रस्तुत पुस्तक पर शोध कार्य करने से इस पुस्तक से सम्बन्धित तथ्य अध्येताओं के सम्मुख आयेंगे तथा इस पुस्तक के महत्त्व का आकलन हो सकेगा । अब आप समझ गये होंगे कि इस भाग में हमें क्या दर्शाना है । शोध शीर्षक के अनुरूप शोधकार्य का फल भी होना चाहिए ।
शोध प्रारूप का यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण भाग है । प्राक्कल्पना का अर्थ होता है पूर्व में कल्पना करना । अपने शोध शीर्षक के विषय में हम यह बताते हैं कि यह शोधकार्य किस प्रकार से अपने मूलभूत विषय का उपस्थापन करेगा अथवा इस विषय पर हमारे शोधकार्य से किस प्रकार के प्रतिफल के आने की सम्भावना है । इस बात का वर्णन भी इस शोधप्रारूप में करना पड़ता है ।
इस भाग में यह लिखना होता है कि आपके शोध-शीर्षक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ? इस शीर्षक से सम्बन्धित तथ्यों का इतिहास क्या रहा है ? आपके शीर्षक को प्रभावित करने वाले कैसे-कैसे ग्रन्थ या कैसी-कैसी साहित्यिक सामग्री पूर्वकाल से ही उपलब्ध है अथवा प्राचीनकाल में आपके शोधविषय का प्रारूप क्या था ? इस भाग में शोध शीर्षक का ऐतिहासिक विवरण देना चाहिए ।
7. शोध-सर्वेक्षण(research survey)
शोधप्रारूप का यह भाग अतीव महत्त्वपूर्ण होता है । आपने कोई भी शोध शीर्षक चुन तो लिया, शोध प्रारूप भी बना लिया , सब कुछ निश्चित हो गया कि इसी शोध विषय पर हमें कार्य करना है परन्तु बाद में कमेटी में जाकर खारिज हो गया तथा पत्र में लिखकर आ गया कि जिस विषय पर आप शोधकार्य करने जा रहे हैं उस विषय पर तो कार्य हो चुका है । तब आपका मुंह देखने लायक होता है । तो यह घटना आपके साथ घटे इससे पूर्व ही यह निरीक्षण कर लें कि जिस विषय का आपने चुनाव किया है वह अकर्तृक है अर्थात् उस पर किसी ने शोध कार्य नहीं किया है । अपने शोध प्रारूप के इस भाग में आप यही बताएंगे कि जिस विषय पर मैं शोध कार्य करने जा रहा हूँ उस विषय पर मेरे संज्ञान में कोई शोधकार्य नहीं हुआ है । इसका सर्वेक्षण हमने कर लिया है तथा यह शोध शीर्षक शोधकार्य हेतु अर्ह है ।
8. शोध-प्रकृति(nature of research)
इस भाग में आप यह बताते हैं कि आपने अपने शोधकार्य में किस विधि या किस शोध पद्धति का इस्तेमाल किया है । आपके शोध की प्रकृति क्या है ? इस विषय में आप निश्चय करते हैं कि हमने शोधकार्य की परिपूर्णता एवं स्पष्टता हेतु किन-किन विधियों का समावेश किया है । यह प्रकृति अनेक प्रकार की हो सकती है । शोधकार्य में कहीं तुलनात्मक, कहीं विश्लेषणात्मक या कहीं विमर्शात्मक या कहीं-कहीं अन्यान्य शोध-प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है । इन्हीं विषयों की सम्भावना प्रस्तुत भाग में करनी चाहिए ।
शोध-प्रविधियों की जानकारी के लिए देखें- शोध-प्रविधियाँ ।
9. अध्याय-विभाजन(chapter division)
इस भाग में आप अपने शोधकार्य का प्रबन्ध भाग दर्शाने हेतु अध्याय विभाजन करते हैं । आपके शोध- प्रबन्ध के अध्यायों का प्रारूप कैसा रहेगा उन बातों का विवरण आप इस भाग में लिखेंगे । आपके शोध प्रबन्ध में 5,6,7,8,9, या 10 कितने अध्याय होंगे इसका स्पष्ट उल्लेख यहां होना चाहिए ।
अध्याय विभाजन में ध्यातव्य बातें-
- अध्यायों की संख्या आपके शोध प्रबन्ध के अनुरूप होनी चाहिए ।
- फालतू अध्याय न जोड़ें जिसका आपके शोध प्रबन्ध में कोई महत्त्व न हो ।
- अध्यायों में विशिष्ट तथ्यों से सम्बन्धित सब-टाइटल(sub-title) का प्रयोग करें ।जैसे-
अध्याय.1 के अन्तर्गत 1.1,1.2,1.3,...आदि या(क),(ख),(ग)... इत्यादि ।
- अध्याय विभाजन में सर्वप्रथम भूमिका फिर अध्यायों का क्रम पुनः उपसंहार अन्त में परिशिष्ट की योजना करनी चाहिए ।
10. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची(reference bibliography)
शोध प्रारूप का यह अन्तिम भाग है । इस भाग में आपके शोध विषय में प्रयुक्त ग्रन्थों की जानकारी यहाँ देनी पड़ती है । सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में ग्रन्थ के लेखक, रचयिता या सम्पादक का नाम, ग्रन्थ का नाम या शीर्षक, प्रकाशक का नाम , प्रकाशन स्थल , संस्करण एवं वर्ष का क्रमशः उल्लेख करना चाहिए । पत्र-पत्रिकाओं या इन्टरनेट की भी यदि सहायता ली गई है तो इसका भी उल्लेख आप यहाँ कर सकते हैं ।
सबसे अन्त में नीचे बाएँ दिनाङ्क एवं स्थान का सङ्केत करना चाहिए तत्पश्चात् उसके नीचे बाँए ही साइड मार्गदर्शक का नाम एवं दायें अपना नाम एवं हस्ताक्षर अङ्कित करना चाहिए ।
हमें आशा है आपको यह लेख पसन्द आयेगा । आपको यह लेख कैसा लगा इसके बारे में कमेन्ट बॉक्स में लिखकर हमें प्रेषित करें । यदि सम्बन्धित विषय में किसी प्रकार की आशंका है तो भी कॉमेन्ट करके अवश्य सूचित करें ।
शोध प्रारूप पीडीएफ डाउनलोड
यह भी पढ़ें>>>
- शोध का अर्थ, परिभाषा, तत्व, महत्व, प्रकार, चरण और शोध प्रारूप/design ,
- शोध प्रबन्ध(Thesis) कैसे लिखें ?, शोध प्रबन्ध की रूपरेखा और महत्व
- शोध प्रस्ताव(Research Proposal) क्या है ? अर्थ, उद्देश्य, महत्व और रूपरेखा
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत अनुसंधान की प्रकृति(Reseach Area In Modern Age)
- Sanskrit Research methodology video ppt in Sanskrit
- अथर्ववेद का चिकित्साशास्त्र : एक अध्ययन
- भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण ,
- बलाघात : अर्थ एवं प्रकार ,
- अक्षर ध्वनियाँ एवं भेद ,
- ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाएँ ,
- स्वर तथा व्यञ्जन ; अर्थ, एवं वर्गीकरण,
- भाषाशास्त्रियों के महाभाष्य सम्बन्धी मत का खण्डन ,
- ध्वनि वर्गीकरण के सिद्धान्त एवं आधार ,
- भाषाऔर बोली : अर्थ एवं भेद ,
- वैदिक और लौकिक संस्कृत में भेद ,
- भाषा विज्ञान एवं व्याकरण का सम्बन्ध ,
- भाषा उत्पत्ति के अन्य सिद्धान्त ,
- भाषा उत्पत्ति के सिद्धान्त । वेदों का अपौरुषेयत्व एवं दिव्योत्पत्तिवाद ,
- भाषा क्या है? भाषा की सही परिभाषा

SOORAJ KRISHNA SHASTRI
You might like, एक टिप्पणी भेजें.
22टिप्पणियाँ
महादय: शोधप्रारूपस्य उत्तमम् रित्याम् विवरणं दत्तवान्। शोधर्थि कृत्ते उपयोगि भवेत्।

धन्यवाद, यदि आप सभी के काम आ सकूँ तो स्वयं को सफल मानूँगा। यदि आप इससे लाभान्वित हुए हों तो और मित्रों को भी प्रेरित करें ।
Thank you sir ek synopsis bhej dijiye koi ho apke pass toh
Koi AK synopsis bhejen sir
Thanks Sir 🙏

बहुत अच्छा विवरण। इस सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जा सकता है?
जी हाँ हमसे सम्पर्क करने के लिए हमारे ईमेल आईडी [email protected] या फोन नंबर 7376572355 पर सम्पर्क कर सकते हैं धन्यवाद 🙏🙏
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने एक एक चरण को बेहतर ढंग से समझाया हैं 🙏🙏
धन्यवाद भाई 🙏🙏
Bahut hi sundar prasentation sir..
Babu ki sundar lekh dhanyavad
बहुत ही सुंदर जानकारी
Thank you for giving this a beautiful information for synopsis of PhD
अतिउत्तम प्रस्तुति एवं बहुपयोगी लेख
It's very useful and helpful for my synopsis 🙏
Thank you🙏🙏
Sir readymade शोधप्रारूप Ka pdf mil Sakta h 5 September last date
Thanks for sharing
very informative post for research. thanks for shering
Bharat mein madhyamik Shiksha ki samasya per shodh

Made with Love by
- Privacy Policy
#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)
Contact form.


अनुसंधान प्ररचना के प्रकार | Types of Research design in Hindi
अनुसंधान प्ररचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
अनुक्रम (Contents)
अनुसंधान प्ररचना के प्रकार
सामाजिक अनुसंधान प्ररचना प्रमुख रूप से निम्नलिखित चार प्रकार की होती है-
1. अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक प्ररचना –
जब शोधकर्ता किसी ऐसे विषय का शोध करता है जिसमें उपकल्पना का निर्माण कठिन होता है, तब अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का निर्माण किया जाता है। जैसा कि सेल्ट्जि ने लिखा है, “अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना उस अनुभव का प्राप्त करन क लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान के हेतु सम्बद्ध प्राकल्पना के निरूपण में सहायक होगा।” शोध के विषय के चयन के उपरान्त प्राकल्पना के निर्माण में इस प्रकार की प्ररचना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शोध प्ररचना द्वारा किसी सामाजिक घटना अथवा परिस्थिति के अन्तर्निहित कारणों की खोज की जा सकती है। सामाजिक अनुसन्धान में अन्वेषणात्मक अध्ययन का महत्व उसके कार्यों के कारण है। अन्वेषणात्मक अध्ययन में सात प्रमुख प्रयोग या कार्य हैं, जो निम्नलिखित प्रकार हैं-
(1) पूर्व निर्धारित उपकल्पना का तात्कालिक स्थितियों के सन्दर्भ में परीक्षण करना। (2) विभिन्न अनुसन्धान-प्रणालियों के प्रयोग की सम्भावनाओं का स्पष्टीकरण करना। (3) सामाजिक महत्व की समस्याओं की ओर अनुसन्धानकर्ता को प्रेरित करना। (4) अनुसन्धान-कार्य को प्रारम्भ करना। (5) विज्ञान की सीमाओं में विस्तार करके उसके क्षेत्र का विकास करना।
2. वर्णनात्मक प्ररचना/अभिकल्प –
विषय या समस्या के सम्बन्ध में सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों के आधार पर उनका विस्तृत वर्णन करना ही वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प है। इस पद्धति में आवश्यक है कि हमें वास्तविक तथ्य प्राप्त हों तभी हम उसकी वैज्ञानिक विवेचना करने में सफल हो सकते हैं। यदि समाज की किसी समस्या का विवरण देना है, तो उस समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त होने चाहिए, जैसे- निम्न श्रेणी के परिवारों का विवरण देना है, तो उसकी आयु, सदस्यों की संख्या, शिक्षा का स्तर, व्यावसायिक ढाँचा, जातीय और पारिवारिक संरचना आदि से सम्बन्धित तथ्य जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक हम उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना अनुसंधान-अभिकल्प विषय के उद्देश्य के अनुसार बनायें।
वर्णनात्मक प्ररचना के चरण (Steps of Descriptive Design) –
(i) अध्ययन के उद्देश्यों का निरूपण – सर्वप्रथम खोज से सम्बन्धित मौलिक प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, ताकि असम्बद्ध तथ्यों का संकलन न हो और अभिनति (Bias) से अध्ययन सुरक्षित भी रहे। अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट कर देने से ये दोनों बातें सम्भव हैं।
(ii) तथ्य-संकलन पद्धति की रूपरेखा – अध्ययन के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करने के उपरांत आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए अध्ययन-पद्धति का चुनाव किया जाता है। भित्र- भिन्न अनुसंधान-पद्धतियों के अपने-अपने गुण हैं। समस्या तथा उद्देश्य के अनुसार सूचना संकलन के लिए सर्वाधिक सहायक प्रणालियों का चुनाव अध्ययन की प्रारम्भिक सफलता है।
(iii) निदर्शन का चुनाव – समूह के प्रत्येक सदस्य का अध्ययन करना अत्यन्त कठिन होता है, अतः समस्त जनसंख्या की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके समग्र समूह के दृष्टिकोणों और व्यवहार के स्वरूपों की व्याख्या की जाती है। इन प्रतिनिधि इकाइयों के चुनाव अर्थात निदर्शन के चुनाव में भी अभिनति से बचाव रखना आवश्यक है।
(iv) सामग्री का संकलन तथा पड़ताल – सामग्री संकलन का कार्य वर्णनात्मक अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साक्षात्कारकर्ता अथवा अवलोकनकर्ता की ईमानदारी तथा परिश्रम से ही शुद्ध तथा यथार्थ सूचनायें एकत्रित की जा सकती हैं, अतः सामग्री संकलन के समय भी कार्यकर्ताओं का नियमित निरीक्षण होते रहना चाहिए। एकत्रित सामग्री की जांच- पड़ताल भी अत्यन्त आवश्यक कार्य है। विश्वसनीयता, स्पष्टता, सम्पूर्णता तथा निरंतरता के लिए संकलित सूचना की पड़ताल वर्णनात्मक अध्ययन का महत्वपूर्ण चरण है।
(v) परिणामों का विश्लेषण – परिणामों के विश्लेषण का अर्थ है, संकलित सामग्री का समूहों के अनुसार वर्गीकरण, सारणीयन तथा सांख्यिकीय विवेचन, आदि। शुद्धता तथा परीक्षण इस कार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकतायें हैं। अतः सारणीयन तथा सांख्यिकीय विवेचन में तो प्रमुख रूप से निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
(vi) प्रतिवेदन/विज्ञप्तिकरण – परिणामों के विश्लेषण के पश्चात् विज्ञप्ति के रूप में निष्कर्षों का प्रकाशन भी किया जाता है।
3. निदानात्मक प्ररचना-
सामाजिक अनुसंधान मूल रूप से दो प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित है। एक तो सामान्य सामाजिक नियमों की खोज करने तथा दूसरी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के समाधान से सम्बन्धित हैं निदानात्मक अध्ययन वे अध्ययन हैं जो किसी विशिष्ट समस्या के निदान की खोज करते हैं निदानात्मक अध्ययन में समस्या का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
निदानात्मक अध्ययन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं-
(1) निदानात्मक अध्ययन, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट है केवल प्राप्ति के उद्देश्य से नही होता, अपितु किसी सामाजिक परिस्थिति के उपचार से सम्बन्धित होता है।
(2) उपचार अथवा निदान प्रस्तुत करने के लिये लक्षण अथवा परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले कारकों का पता लगाना अनिवार्य है। अतः निदानात्मक अध्ययन कारकों का भी अध्ययन करता है।
(3) निदानात्मक अध्ययन सामाजिक ढाँचे तथा सामाजिक सम्बन्धों से उत्पन्न उन सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित रहता है. जिनको दूर करना तत्काल आवश्यक होता है।
(4) निदानात्मक अध्ययन एक स्पष्ट तथा निश्चित उपकल्पना के द्वारा संचालित होता है। वास्तव में, निदानात्मक अध्ययन का तात्कालिक उद्देश्य होता हे और यह वर्णनात्मक अध्ययन के बाद की कड़ी है।
4. परीक्षात्मक अथवा प्रयोगात्मक प्ररचना-
भौतिक विज्ञानों की भाँति निश्चित, स्पष्ट तथा यथार्थ परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक समस्याओं की प्ररचनाओं में परीक्षणात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर बहुत बल दिया जा रहा है। परीक्षण की परिभाषा करते हुए ऐकॉफ ने कहा है- “परीक्षण एक क्रिया है और ऐसी क्रिया है जिसे हम पूछताछ कहते हैं।”
चेपिन के अनुसार, ‘समाजशास्त्रीय अनुसंधान में परीक्षणात्मक प्ररचना की धारणा नियंत्रण की दिशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव-सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है।
Important Links
- आदिम/ जनजातिय धर्म क्या है? टाइलर के धर्म सम्बन्धी विचार | Meaning of tribal religion and ideas of Taylor’s religion in Hindi
- नातेदारी की परिभाषा एवं इसके प्रमुख भेद
- नातेदारी व्यवस्था में ‘परिहास’ सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए। ( Avoidance relations in kinship system)
- जनजातीय परिवार का अर्थ तथा इसकी विशेषताएं- Meaning of tribe family & it characteristics in Hindi
- जनजातीय सामाजिक संगठन | Social Organisation of tribe in Hindi
- भारतीय जनजातियों के भौगोलिक वर्गीकरण | Geographical classification of Indian tribes
- सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासवादी सिद्धान्त का आलोचनात्मक | Evolutionary Theory of social Change in Hindi
- संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता तथा इसकी सीमाएं -sociology in Hindi
- संस्कृति और समाज में सम्बन्ध | Relationship between in culture & society in Hindi
- सामाजिक प्रतिमानों की अवधारणा तथा उसकी विशेषताएँ एवं महत्व | Concept of social models
- मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा और इसके प्रकार | Concept of Power & its Variants
- मैक्स वेबर के आदर्श-प्रारूप की धारणा | Max Weber’s Ideal Format Assumption in Hindi
- स्पेन्सर के सामाजिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद | Historical Evolutionism in Hindi
- स्पेन्सर के समाज एवं सावयव के बीच समानता | Similarities between Spencer’s society & matter
- मार्क्स के वर्ग-संघर्ष सिद्धांत | Marx’s class struggle Theory in Hindi
- आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था में मार्क्स के वर्ग-संघर्ष | Modern capitalist system in Hindi
- अगस्त कॉम्टे के ‘प्रत्यक्षवाद’ एवं कॉम्टे के चिन्तन की अवस्थाओं के नियम
- आगस्ट कॉम्टे ‘प्रत्यक्षवाद’ की मान्यताएँ अथवा विशेषताएँ | Auguste Comte of Positivism in Hindi
- कॉम्ट के विज्ञानों के संस्तरण | Extent of Science of Comte in Hindi
- कॉम्ट के सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान – social dynamics in Hindi
- सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा और इसकी प्रकृति Social Survey in Hindi
- हरबर्ट स्पेन्सर का सावयवि सिद्धान्त एवं सावयवि सिद्धान्त के विशेषताएँ
- मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical materialism) की विशेषताएँ
- द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (कार्ल मार्क्स)| Dialectical materialism in Hindi
You may also like

प्रसार शिक्षा के भौतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का...

प्रसार शिक्षा के सांस्कृतिक एवं सामुदायिक उद्देश्य
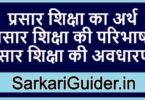
प्रसार शिक्षा का अर्थ | परिभाषा | अवधारणा
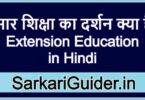
प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है? | Extension Education...

सामाजिक संगठन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, लक्षण या...

सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषा | सामाजिक संगठन एवं...
About the author.
Sarkari Guider Team
Leave a comment x.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Contents in the Article
अनुसंधान का अर्थ ( Meaning of Research)
अनुसंधान के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। यह उत्तर मानवीय प्रयासों पर आधारित होता है इस प्रत्यय को चन्द्रमा के एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले जब तक मनुष्य चन्द्रमा पर नहीं पहुँचा था, चन्द्रमा वास्तव में क्या हैं ? इस सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं थी। यह एक समस्या भी थी जिसका कोई समाधान भी नहीं था। मनुष्य को चन्द्रमा के सम्बन्ध में मात्र आवधारणाएं ही थी, शुद्ध ज्ञान नहीं था। परन्तु मनुष्य अपने प्रयास से चन्द्रमा पर पहुंच गया है। इस प्रकार शोध कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है अथवा मनुष्य की जानकारी में नहीं है। उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाता है जिसका समाधान उपलब्ध नहीं है और न ही मनुष्य की जानकारी में है।
अनुसंधान की परिभाषा ( Definition of Research)
अनेक परिभाषाएं अनुसन्धान की गई है प्रमुख परिभाषा इस प्रकार हैं-
रेडमेन एवं मोरी के अनुसार- “नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यावस्थित प्रयास ही अनुसंधान हैं।”
पी० एम० कुक के अनुसार- ‘अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी, एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है। जिसमें तथ्यों, सिद्धान्तों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसंधान की उपलिब्ध तथा निष्कर्ष प्रामाणिक तथा पुष्टि करने योग्य होते हैं। जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है।
उद्देश्य ( Objectives of Research)
शोध समस्याओं की विविधता अधिक है इसके चार प्रमुख उद्देश्य होते हैं- सैद्धान्तिक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य तथा व्यावहारिक उद्देश्य इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
- सैद्धान्तिक उद्देश्य ( Theoretical Objectives)- अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध कार्य द्वारा नये सिद्धान्तों तथा नये नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार के शोध कार्य में अर्थापन होता है। इसमें चरों के सम्बन्धों को प्रगट किया जाता है और उनके सम्बन्ध में सामान्यीकरण किया जाता है। इससे नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, जिनका उपयोग शिक्षण तथा निर्देशन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है।
- तथ्यात्मक उद्देश्य ( Factual Objectives)- शिक्षा के अन्तर्गत ऐतिहासिक शोध-कार्यो। द्वारा नये तथ्यों की खोज की जाती है। इनके आधार पर वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। इन उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। क्योंकि तथ्यों की खोज करके, उनका अथवा घटनाओं का वर्णन किया जाता है। नवीन तथ्यों की खोज शिक्षा-प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में सहायक होती है, निर्देशन प्रक्रिया का विकास तथा सुधार किया जाता है।
- सत्यात्मक उद्देश्य ( Establishment of Truth Objective)- दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। इनकी प्राप्ति अन्तिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। दार्शनिक शोध-कार्यों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धान्तों तथा शिक्षण विधियों तथा पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। शिक्षा की प्रक्रिया के अनुभवों का चिन्तन बौद्धिक स्तर पर किया जाता है। जिससे नवीन सत्यों तथा मूल्यों को प्रतिपादन किया जा सकता है।
- व्यावहारिक उद्देश्य ( Application Objectives)- शैक्षिक अनुसंधा निष्कर्षों का व्यावहारिक प्रयोग होना चाहिए। परन्तु कुछ शोध-कार्यों में केवल इन्हें विकासात्मक अनुसन्धान भी कहते है। क्रियात्मक अनुसन्धान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है अर्थात् इनका उद्देश्य व्यावहारिक होता है। स्थानीय समस्या के समाधान से इसका उपयोग अधिक होता है। स्थानीय समस्या के समाधान से भी इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। निर्देशन में इसकी उपयोगिता अधिक होती है।
अनुसन्धान का वर्गीकरण (Classification of Research)
अनुसन्धान के उद्देश्यों से यह स्पष्ट है कि अनुसन्धानों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। प्रमुख वर्गीकरण मानदण्ड पर आधारित है-
योगदान की दृष्टि से (Contribution Point of View)
शोध कार्यों के योगदान की दृष्टि से शैक्षिक अनुसन्धानों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-
मौलिक अनुसंधान ( Basic or Fundamental Research)- इन शोध कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है-नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन नवीन तथ्यों की खोज, नवीन तथ्यों का प्रतिपादन होता है। मौलिक-अनुसन्धानों से ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। इन्हें उद्देश्यों की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जा सकता है-
- प्रयोगात्मक शोध-कार्यों से नवीन सिद्धान्तों तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। सर्पक्षण शोध से इसी प्रकार का योगदान होता है।
- ऐतिहासिक शोध कार्यो से नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। जिनमें अतीत का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है।
- दार्शनिक शोध कार्यों से नवीन सत्यों एवं मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शिक्षा का सैद्धान्तिक दार्शनिक अनुसन्धानों से विकसित किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- निर्देशन (Guidance)- अर्थ, परिभाषा एवं विशेषतायें, शिक्षा तथा निर्देशन में सम्बन्ध
- सूक्ष्म-शिक्षण- प्रकृति, प्रमुख सिद्धान्त, महत्त्व, परिसीमाएँ
- निर्देशन के उद्देश्य (Aims of Guidance in Hindi)
- शैक्षिक निर्देशन (Educational Guidance)-परिभाषा, विशेषताएँ, सिद्धान्त
- शैक्षिक निर्देशन-उद्देश्य एवं आवश्यकता (Objectives & Need)
- व्यावसायिक निर्देशन (Vocational guidance)- अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा का व्यावसायीकरण
- परामर्श (Counselling)- परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, विशेषताएँ
- विशेष शिक्षा की आवश्यकता | Need for Special Education
- New Education Policy- Characteristics & Objectives in Hindi
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 की संकल्पनाएँ या विशेषताएँ- NPE 1992
- सूक्ष्म शिक्षण- परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, प्रतिमान, पद
- व्यावसायिक निर्देशन- आवश्यकता एवं उद्देश्य (Need & Objectives)
Disclaimer: wandofknowledge.com केवल शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, अस्वीकरण से अनुरोध है कि कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम नकल को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अगर किसी भी तरह से यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है, तो कृपया हमें [email protected] पर मेल करें।
About the author
Wand of Knowledge Team
बहुत सुन्दर प्रस्तुति। सम्पूर्ण जानकारी देने में सक्षम है।
Leave a Comment X
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
DSpace JSPUI
Egyankosh preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets.
- IGNOU Self Learning Material (SLM)
- 02. School of Social Sciences (SOSS)
- Master's Degree Programmes
- Master's in Anthropology (MAAN)
- MANI-001 Anthropology And Method of Research
- Block-3 Research Design
Items in eGyanKosh are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


IMAGES
VIDEO
COMMENTS
3. सांख्यिकीय प्ररचना (Statistical Design) - इसका सम्बन्ध संकलित सामग्री के सांख्यिकीय विश्लेषण से है अर्थात यह पूर्व निर्णय लेने से है कि सामग्री के विश्लेषण हेतु ...
Research Design in Research Methodology, research design in hindi, Features of good research design, Use of Good Research Design, Research Proposal: https://...
#Marketing_Research #Marketing_Research_BBA #Marketing_Research_MBA In this video you will get to know about Concept and types of Research Design in very eas...
Research Design: Concept, Meaning and Features | Quickest & Easiest Explanation in HindiA research design is a conceptual structure within which a research i...
Research design in Hindi के लिए PPT नीचे दी गई है-Research design and types of research design final ppt from Prahlada G Bhakta. FAQs. रिसर्च डिज़ाइन के लाभ कौन कौन सी है?
अनुसंधान. व्यापक अर्थ में अनुसन्धान (Research) किसी भी क्षेत्र में 'ज्ञान की खोज करना' या 'विधिवत गवेषणा' करना होता है। वैज्ञानिक अनुसन्धान ...
10. सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची (reference bibliography) शोधप्रारूप या सिनॉप्सिस (synopsis) के यही दस चरण हैं जिससे शोधप्रारूप का निर्माण होता है । अब हम आगे ...
Article. Jan 1973. F. N. Kerlinger. Request PDF | On Dec 26, 2016, Patanjali Mishra published शोध अभिकल्प का अर्थ एवं उद्देश्य Meaning and ...
वर्णनात्मक प्ररचना के चरण (Steps of Descriptive Design) - (i) अध्ययन के उद्देश्यों का निरूपण - सर्वप्रथम खोज से सम्बन्धित मौलिक प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है ...
PDF | On Dec 26, 2016, Patanjali Mishra published इकाई-7 शोध समया क परभाषा एवं शोध समया चु नने का आधार (Definition of ...
24 lessons • 5h 7m. 1. Overview Of The Course - Methodology Of Sociological Research (in Hindi) 3:53mins. 2. Meaning And Difference Between Social And Sociological Research (in Hindi) 15:00mins. 3. Nature Of Social Phenomenon (in Hindi)
Descriptive Research Design in hindi, Descriptive research design type, cross sectional research, longitudinal research,Exploratory Research Design :https://...
Different Research Design (in Hindi) 5:19mins. 6. Developing a Research Plan (in Hindi) 5:20mins. 7. Sample Design (in Hindi) 6:09mins. Crack NTA-UGC-NET & SET Exams with Unacademy Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Structured syllabus. Daily live classes.
अनुसंधान का अर्थ (Meaning of Research) अनुसंधान की परिभाषा (Definition of Research) उद्देश्य (Objectives of Research) अनुसन्धान का वर्गीकरण (Classification of Research) योगदान की दृष्टि से ...
research design meaning in Hindi. research design. meaning in Hindi. 1. Randomized field experiments are the strongest research designs for assessing program impact. 2. Environmental variables can also influence results and usually arise from poor research design. 3.
यह विडिओ Descriptive Research Design को विस्तार से वर्णित करता है। इसे उपयुक्त उदाहरणों के ...
DSpace JSPUI eGyanKosh preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Different Research Design (in Hindi) 5:19mins. 6. Developing a Research Plan (in Hindi) 5:20mins. 7. Sample Design (in Hindi) 6:09mins. Crack NTA-UGC-NET & SET Exams with Unacademy Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Structured syllabus. Daily live classes.
Get access to the latest Research Design - Meaning And purpose (in Hindi) prepared with NTA-UGC-NET & SET Exams course curated by Dr Malvika Kandpal on Unacademy to prepare for the toughest competitive exam. ... Sociology. Basic Concepts and Institutions. Research Design - Meaning And purpose (in Hindi) Lesson 13 of 24 • 6 upvotes • 12 ...
research methodologydata collection methods in researchresearch designmarketing researchtypes of research design#researchdesign #marketingresearch #researchm...
A research design is a strategy for answering your research question using empirical data. Creating a research design means making decisions about: Your overall research objectives and approach. Whether you'll rely on primary research or secondary research. Your sampling methods or criteria for selecting subjects. Your data collection methods.
99 lessons • 13h 23m. 1. Research Aptitude- Course Over View (in Hindi) 6:07mins. 2. Part 1 Research Aptitude Basic Terms (in Hindi) 9:22mins. 3. Part 2 Research Aptitude Basic Terms (in Hindi)
research methodologydata collection methods in researchresearch designmarketing researchtypes of research design#researchdesign #marketingresearch #researchm...